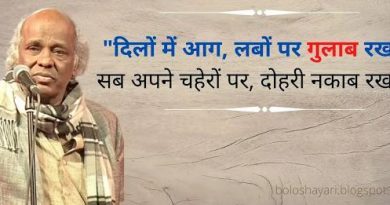पत्रकार कमल पर हमले के बहाने… चाहे रमन हों या भूपेश दोनों की सरकारों में ज्यादा कुछ जमीन पर नहीं बदला …
नेशन अलर्ट / 97706 56789
सुरेश महापात्रा
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर हमले की यह कोई पहली या अंतिम कड़ी नहीं है। नए प्रदेश के गठन के बाद से अब तक बीते दो दशक में ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जब पत्रकारिता चोटिल हुई है।
लिखने वाले मारे गए, नक्सल मामले में फंसाए गए, नक्सलियों ने हत्या की, पुलिस ने फर्जी केसों में उलझा दिया। अखबार के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया गया। राजनीतिक, प्रशासनिक, पुलिस और नक्सल के खौफ के साए में पत्रकारिता कूलांचे मारती रही… हर हादसे के बाद बड़े अखबारों में करोड़ों खर्च कर सरकार के फेसवॉश का साक्षी भी यह प्रदेश रहा है।
चाहे रमन हों या भूपेश दोनों की सरकारों में ज्यादा कुछ जमीन पर नहीं बदला है। वही अफसरशाही, वही राजनैतिक कार्यकर्ता का दंभ साक्षात है।
हां, भूपेश सरकार ने दो सक्रिय पत्रकारों को अपनी टीम में पहले ही दिन से जगह देकर एक नई राह की आस जगाई। ऐसे में, अब होने वाले हादसों को लेकर इनकी सरकार में भूमिका तलाशा जाना नाजायज़ तो नहीं होना चाहिए।
कमल शुक्ला के साथ जो हुआ यह सभी ने देखा। पूरा देश उद्वेलित है मीडिया पर हमले को लेकर चिंता साफ देखने को मिल रही है। पर असल में मसले की बारिकी को भी देखना समझना होगा।
कांकेर में यह कोई एक दिन में होने वाली अनायास घटना नहीं है। यह सुनियोजित तरीके से अंजाम दिए जाने वाली घटना है। विवाद के शुरूआत में इसके नेपथ्य में कांकेर के जिला अधिकारी की भूमिका है।
वाट्सएप के चैट से निकली बात सड़क पर हाथापाई तक पहुंची है। यह समझने की दरकार है। मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी कांकेर के हैं। वे मर्म को करीब से समझते होंगे और सीएम को जिला अधिकारी से ज्यादा उनकी बातों पर विश्वास होना चाहिए। यह मेरी समझ का विषय है। पर यदि दोनों तरफ से पेश तथ्य एकतरफा सत्य पर आधारित होंगे तो कोई मसले का हल नहीं तलाश सकता।
अक्सर मीडिया कर्मी से जुड़े हर मामले में प्रथमत: यही होता रहा है। यही होता रहेगा। सबसे पहले मीडियाकर्मी का दोष तलाशने की जुगत फिर कारण पर नज़र। इसके बाद बचने-बचाने की कोशिश। मीडिया कर्मी आपस में भी उलझते रहे हैं।
मामला थाना-कचहरी तक पहुंचता है। वे आपस में ही बैठकर अपने मसले सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुलझ जाए तो ठीक नहीं तो न्यायालय ही गुण-दोष का निर्धारण करता रहा है। कमोबेश यह अवस्था बहुत से मीडियाकर्मियों की जिंदगी में आती रही है। यह सब कुछ खबरों के चक्कर में होता है।
किसी दूसरे यानी राजनैतिक दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अफसर या व्यापारी (ठेकेदार, सप्लायर) को हक नहीं है कि वह पक्षकार बनकर पत्रकार पर जानलेवा हमला करे, फंसाने की साजिश करे या नुकसान पहुंचाए।
अब के दौर में यही ज्यादातर मामलों में हो रहा है। ज्यादातर पत्रकार अब पक्षकार की हैसियत में रहने की आदत डालने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये पत्रकारिता उस लूट में हिस्सेदारी को लेकर होती है जिसमें पत्रकार भाग्योदय की संभावना तलाश रहा होता है।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मीडिया हाउस की वह भूमिका जिसमें उसके द्वारा दी जाने वाली कीमत है। 95 फीसदी पत्रकार स्वयं के जोखिम पर काम करते हैं। संस्थान यदि प्रेस कार्ड दे दिया तो बड़ी बात। अब तो ऐसा करने में भी झिझक बढ़ गई है।
आर्थिक स्वालंबन के लिए अवैतनिक मीडिया कर्मी साइड बिजनेस करने लगता है। इसमें सभी सही काम ही कर रहे हों यह जरूरी नहीं। यहीं से शुरू होती है दोराहा…
एक ओर कमल जैसे खड़े होते हैं दूसरी ओर मीडिया का लबादा ओढ़ा वह चेहरा जो जरूरत के हिसाब से पार्टी का पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ठेकेदार भी बन जाता है…
पत्रकार के साथ विवाद के बाद यह जरूरत के हिसाब से चेहरा दिखाता है। जो व्यक्ति मीडिया में है पर वह सरकार के अनुशांगिक अंगों ठेकेदारी, सप्लाई और राजनीतिक कार्यकर्ता है वह हर तरह से उपयोग के लायक होता है। यही वह कड़ी है जो परेशान कर रहे पत्रकार को ठिकाने लगाने में सत्ता की सहायता भी करता है।
कमल के साथ कांकेर में यही हुआ है। सरकार कमल के नखरों से खुश रह ही नहीं सकती। वह कहीं भी कुछ भी कह देता है… अड़ जाता है… लड़ जाता है…
सो कांटे से कांटा निकाल फेंकने के सूत्र का यह प्रयोग, संयोग मात्र नहीं है। यह असल में एक सिंडिकेट के विरूद्ध लड़ाई का नतीजा है जिसमें दोनों पक्षों में नेकनीयति का नितांत अभाव है।
अंत में कमल पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौर में आंख की किरकिरी थे। अब भी हैं। निश्चित तौर पर आगे भी यही हाल रहेगा। पर कांग्रेस सरकार में यह सडक छाप गुंडागर्दी दक्षिण भारतीय सिनेमा की चुगली करती दिख रही है… ( साभार : सीजी इंपेक्ट )